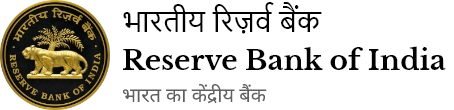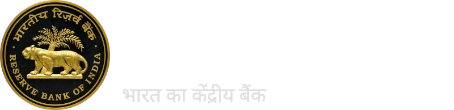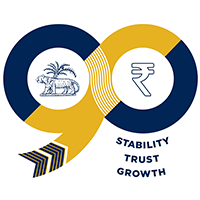IST,
IST,


"इक्कीसवीं शताब्दी में भारत की अर्थव्यवस्था
"इक्कीसवीं शताब्दी में भारत की अर्थव्यवस्था
एक नयी शुरूआत या आभासी उष:काल?"
15 जनवरी 2001
सरकारी और सार्वजनिक वितरण प्रणालियों में कामकाज में जनसाधारण के हित को और न कि सार्वजनिक सेवकों के हित को ध्यान में रखकर किये जानेवाले कानूनी सुधार, सार्वजनिक एजेंसियों को कार्यनिष्पादन के लिए जवाबदेही ठहराये जाने हेतु सुस्पष्ट क्रियाविधि, सूचना की स्वतंत्रता और सरकार तथा उसकी बहुविध एजेंसियों द्वारा वित्त संबंधी लिये जानेवाले निर्णयों को पूरी तरह सामने लाने तथा राजकोषीय अधिकार प्रदान करना ये ऐसे कुछ उपक्रम हैं जो इस वर्तमान मोड़ पर हमारे लिए आवश्यक हैं। अतीत के डरावने अनुभव को देखते हुए अंतिम कार्य सबसे कठिन कार्य था, परंतु अधिक समय तक उसे टाला नहीं जा सकता था। ये विचार भारतीय रिज़र्व बैंक के गवर्नर डॉ. विमल जालान ने दिल्ली में इंडिया इंटरनैशनल सेंटर द्वारा आयोजित 16वें सी. डी. देशमुख मेमोरियल लैक्चर में भाषण देते समय्ा व्यक्त किये।
डॉ. जालान ने कहा कि "हमें एक नये जिम्मेवारी और जवाबदेही के सुस्पष्ट विभाजन पर आधारित सुगठित नयी राजनैतिक अफसरशाही की ज़रूरत है।" उन्होंने इस बात की ओर इशारा किया कि यह दूसरी पीढ़ी के सुधारों का अपेक्षाकृत कठिन हिस्सा है। इस बात को स्पष्ट करते हुए उन्होंने कहा कि आज गैर-सरकारी क्षेत्र के पास अपनी खुद की गतिशीलता और बल है और सेवा क्षेत्र में, भारतीय संस्थाओं, निगमों तथा व्यक्तियों ने विश्व स्तर पर अपवाद रूप से शानदार निष्पादकता का प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि साथ ही साथ यह भी स्पष्ट है कि जब तक हम अपने राजकोषीय फ्रंट को ठीक-ठाक नहीं करते और अपनी सार्वजनिक वितरण प्रणाली में सुधार नहीं लाते, अपने आप में मैक्रो नीतिगत सुधार न तो देर तक टिक सकते हैं और न ही स्थायी परिणाम ही दे सकते हैं। उन्होंने एक उदाहरण देते हुए अपनी बात को आगे बढ़ाय्ाा कि यदि सरकारी एजेंसियों द्वारा चलाये जानेवाले लाखों प्राइमरी स्कूल, जिला प्राधिकारियों द्वारा स्थापित हज़ारों की संख्या में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सैंकड़ों केंद्रीय तथा राज्य विश्वविद्यालय अपनी क्षमता से कम पर काम करते रहें या गिरावट दर्शाते रहें, ऐसे में दो या तीन हाइटैक शहर अथवा एक या दो बिजनेस स्कूल तथा तकनीकी संस्थान मानव संसाधनों की असीम हानि की भरपाई नहीं कर सकतीं" यह सापेक्ष अनुपातों तथा सार्वजनिक हित और निजी प्रगति के बीच जटिल कड़ियों का सीधा सादा मामला है।
आज भारत के पास तरह-तरह के औद्योगिक और उपभोक्ता उत्पादन तथा सेवा पैदा करने तथा प्रोसेस करने के लायक ज्ञान और कुशलता है। दूसरी बात यह है कि यह अंतर्राष्ट्रीय पूंजी गतिशीलता तथा वैश्विक वित्तीय बाज़ारों का एकीकरण भारत के पक्ष में जाते हैं। घरेलू बचतें विकास के लिए महत्त्वपूर्ण बनी हुई हैं। अलबत्ता, घरेलू पूंजी की कमी अब कोई बाध्यकारी अड़चन नहीं रही है। पूंजी की बढ़ती हुई गतिशीलता ने इस बात को सुनिश्चित कर दिया है कि वैश्विक संसाधन उसी देश की तरफ मुड़ेंगे जो वृद्धि का उच्च स्तर दर्शा सकता है और ऊंचे प्रतिफल दे सकता है। अब यह भारत के लिए संभव है कि वह उच्चतर वृद्धि, उच्चतर बाह्य पूंजीगत आगमों तथा उच्चतर देशी आय और बचतों के नैतिकता सम्मत चक्र का लाभ उठाये। डॉ. जालान ने कहा कि ये चीजें वृद्धि को आगे बढ़ा सकती हैं।
अलबत्ता, उन्होंने इस बात की तरफ इशारा किया कि हाल ही के वर्षों के दौरान ‘दूरी की मृत्यु’ और वैश्विक उत्पादन, सेवाओं तथा वित्तीय बाज़ारों के बढ़ते हुए एकीकरण ने न केवल भारत के सामने, बल्कि समूचे विश्व के सामने राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के प्रब्ंध की नयी चुनौतियां खड़ी की हैं। डॉ. जालान का यह भी कहना था कि हाल ही की वैश्विक प्रवृत्तियों का एक और परिणाम यह हुआ है कि राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाएं अपनी खुद की सीमाओं से बाहर की गतिविधियों के आगे बहुत कमज़ोर पड़ रही हैं। उन्होंने तर्क दिया कि "प्रत्यक्ष प्रभावों के अलावा,(जो कि उतार-चढ़ाव वाले स्टॉक बाज़ारों में इस समय बहुत अधिक सुस्पष्ट हैं), संसर्ग के कारण अप्रत्यक्ष प्रभाव भी काफी गम्भीर हो सकते हैं।
डॉ. जालान ने कहा कि इस शताब्दी के प्रारम्भ में हमारे पास दो दिशाओं की चुनौतियां हैं - पहली कि नये अवसरों का लाभ कैसे उठायें और साथ ही साथ, अपने आपको अनाहूत जोखिमों से कैसे बचायें। उन्होने महसूस किया कि संकीर्णता अथवा अलग-थलग हो जाना समस्या का समाधान नही है, क्योंकि इस तरह के नज़रिये से न तो वृद्धि बढ़ेगी और न ही स्थिरता ही। डॉ. जालान का यह मानना था कि आज विश्व अर्थव्यवस्था में जिस तरह के आमूल चूल परिवर्तन हो रहे हैं, और भारत जिस तरह की अपेक्षाकृत बेहतर स्थिति में है, भारत को और अधिक खुला तथा और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की नीतियों की मौजूदा दिशा उचित है और इसे और आगे बढ़ाया जाना चाहिए। इन्होंने तर्क दिया कि जब तक हम अपनी आर्थिक नीतियों में बड़ा परिवर्तन नहीं करते और वैश्विक व्यापार, विदेश तथा प्रौद्योगिकी की समसामयिव वास्तविकताओं के साथ तालमेल बिठाने के प्रयास नहीं करते, भारत के लिए यह संभव नहीं है कि वह सम्मानजनक स्थान पर रह सके और वृद्धि तथा विकास के लिए अपनी पूरी क्षमताओं का दोहन कर सके।
डॉ.जालान का मानना था कि और अधिक तथा गहरे आर्थिक सुधारों की तरफ निर्णायक प्रयास ही भविष्य के लिए पहली कूटनीतिज्ञपूर्ण प्राथमिकता होगी। अलबत्ता, उन्होंने इस बात की चेतावनी दी कि आर्थिक सुधारों की ज़रूरत को यह समझ लेना बहुत बड़ी भूल होगी कि इससे न्यायोचित विकास के लिए सकारात्मक परिवेश तैयार करने और अवसर बढ़ाने के लिए सरकार अथवा सार्वजनिक नीति की भूमिका कम हो जायेगी। भारत जैसे विकासशील देश में, जहां बड़े पैमाने पर अशिक्षा है और आधारभूत ढांचा अविकसित है, वहां सरकार को अवश्य ही शिक्षा, स्वास्थ्य, जल आपूर्ति, सिंचाई, आधारभूत ढांचे आदि जैसे क्षेत्रों में निवेश के ज़रिए वृद्धि के लिए आवश्यक स्थितियां बनाने के लिए महत्त्वपूर्ण तथा अनिवार्य भूमिका निभानी ही चाहिए। ये काम बाज़ार के भरोसे नहीं हो सकते। उन्होंने कहा, "सफल आर्थिक सुधाराें के परिणाम इस रूप में सरकारों की योग्यता बढ़ाने के लिए मिलने ही चाहिए कि वे उच्चतर वृद्धि, उच्चतर राजस्व और उच्चतर उत्पादकता पाने में सहायता करके जो कुछ करना चाहती हैं, उसे कर सकें।" उन्होंने कई संक्रमणकाल की तथा उभरती हुई बाज़ार अर्थव्यवस्थाओं के हाल ही के ऐसे अनुभवों की ओर इशारा किया जिन्होंने यह बात दर्शायी कि आर्थिक सुधार ज़रूरी थे लेकिन वृद्धि और विकास के लिए वे ही पर्याप्त स्थिति नहीं थे।
हमारे आर्थिक जीवन में बढ़ते हुए सार्वजनिक-निजी द्विभाजन पर ध्यान केन्द्रित करते हुए डॉ. जालान ने कहा कि अब आर्थिक नवीकरण तथा सकारात्मक वृद्धि आवेग बड़े पैमाने पर सार्वजनिक क्षेत्र के बाहर हो रहे हैं। बहुत बड़े सरकारी क्षेत्र में न केवल उत्पादन, लाभ तथा सार्वजनिक बचतों के मामले में उल्लेखनीय गिरावट आ रही है, बल्कि ये गिरावट शिक्षा, स्वास्थ्य, जल तथा परिवहन के क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने में भी आ रही है। ये दो तत्त्व - राजकोषीय गिरावट तथा आवश्यक सेवाएं उपलब्ध करा पाने में असमर्थता - आपस में नजदीकी से जुड़ी हुई हैं। उन्होंने बताया कि हमारे अधिकांश सार्वजनिक संसाधन अब वेतनों के भुगतान अथवा पिछले कर्जों पर ब्याज अदा करने में ही खर्च हो जाते हैं और महत्त्वपूर्ण क्षेत्रों में सार्वजनिक अथवा सार्वजनिक समर्थन से चलने वाली सेवाओं के विस्तार के लिए संसाधन बहुत ही कम या बिल्कुल भी नहीं बचते हैं।
डॉ.जालान ने इस बात पर अफ़सोस जाहिर किया कि स्वतंत्र प्रशासन के पचास वर्ष के अनुभव के बाद भी अलग-अलग स्तरों पर सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंध में हमारी समस्याएं और अधिक जटिल होती चली गयी हैं। इस बात को स्पष्ट करते हुए उन्होंने बताया कि न्यायिक प्रक्रियाओं में बाबा आदम के ज़माने से चले आ रहे विलम्ब के बावजूद ‘कानून ही सर्वोपरि’ के लिए हर तरफ सम्मान बना हुआ है। अलबत्ता, ऐतिहासिक कारणों से हमारी विधि प्रणाली तथाकथित ‘सरकारी नौकर’ के निजी हितों को पूरा संरक्षण प्रदान करती है और अक्सर यह संरक्षण उस जनता की कीमत पर होता है जिसकी सेवा के लिए उसे रखा गया होता है। नौकरी की पूरी सुरक्षा के अलावा, किसी भी सरकारी क्षेत्र के संस्थान - अस्पताल, विश्वविद्यालयों, स्कूलों, बैंकों, बसों, डाकघरों, रेलवे, नगरपालिकाओं में सरकारी नौकरों का वोई भी वर्ग - अपने खुद के लिए और अधिक वेतन, पदोन्नति, बोनस की तलाश में हड़ताल पर जा सकता है। भले ही इससे उस जनता को, जिसके नाम पर ही उन्हें वहां भर्ती किया गया है, कितनी भी कीमत क्यों न चुकानी पड़े या असुविधा का सामना न करना पड़े। केन्द्र और राज्यों, दोनों में सरकारों का अपने निर्णय लागू करने का ‘अधिकार’ समय के साथ-साथ क्षीण होता चला गया है। सरकारें अलग-अलग स्तरों पर सामाजिक सेवाएं (जैसे साक्षरता बढ़ाना) के लिए योजनाएं तथा कार्यक्रम घोषित करती हैं लेकिन ये प्रयास राजकोषीय तंगहाली के कारणशुरू ही नहीं हो पाते।
डॉ.जालान ने तर्क किया कि इस राजकोषीय तंगहाली और सार्वजनिक वितरण प्रणालियों के नाकाफी होने के सबसे अधिक असर गरीबों और बेरोजगारों तथा अनपढ़ लोगों पर पड़ते हैं, जो सार्वजनिक सेवाओं, सार्वजनिक निवेश तथा सार्वजनिक कार्यक्रमों पर निर्भर करते हैं। इसका असर निश्चित रूप से समृद्ध वर्गों पर या उन व्यक्तियों पर नहीं पड़ता जो उनकी सेवा करने के लिए चुने या नियुक्त किये जाते हैं। डॉ.जालान ने बताया कि इस नज़रिये को दिमाग में रखना फायदेमंद होगा क्योंकि ‘यथास्थिति’ के पक्ष में काफी अधिक श्रम समाज के कमज़ोर तबकों के नाम पर ही किया जाता है।
इस सन्दर्भ में डॉ.जालान ने इस बात का उल्लेख किया कि आर्थिक सुधारों के अलावा, अब यह बात बहुत महत्त्वपूर्ण है कि सरकार के सभी स्तरों पर - केन्द्र, राज्य तथा ज़िला स्तर पर सरकारी कामकाज तथा सार्वजनिक वितरण प्रणाली में नये सिरे से प्राण पूंकने के लिए तत्काल कार्यक्रम शुरू किये जायें। अकेले सरकार ही जो कुछ कर सकती है, उसे करने की उसकी योग्यता को मज़बूत किये बिना और इसकी गतिविधियों, जो देश के भावी विकास के लिए अत्यधिक महत्त्वपूर्ण हैं, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छ पर्यावरण तथा काम करने वाला आधारभूत ढांचा - पर और अधिक ध्यान दिये बिना भारत अपने सामने उपलब्ध अवसरों का पर्याप्त रूप से दोहन नहीं कर सकता।
सूरज प्रकाश
प्रबंधक
प्रेस प्रकाशनी: 2000-2001/1019
पृष्ठ अंतिम बार अपडेट किया गया: